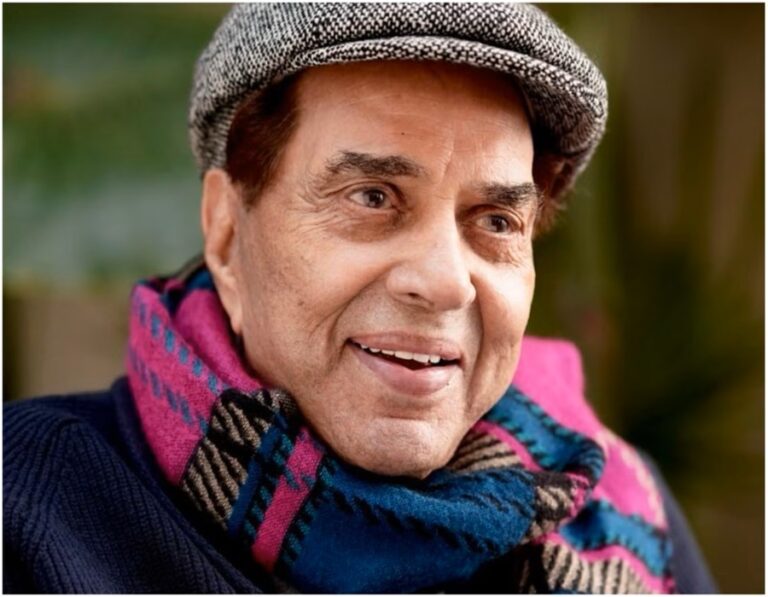ब्रहनिष्ठ संतोष पुरी (स्रोतीय, ब्रहनिष्ठ, परिव्राजक, परमहंस, दशनाम संन्यासी, पुरीनाम, मुल्तानी मढ़ी, बराह देवता, कामाख्या पीठ, रामेश्वरम धाम, महानिर्वाणी अखाड़ा) के विचार
प्रयागराज [TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। कुंभ और वेदों का आपस में क्या तात्विक संबंध है। इसके लिए पहले वेदों के सार को समझना होगा। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि सनातन धर्म में वेदों की क्या भूमिका है। दरअसल, वेद सनातन धर्म की आधारशिला हैं। इन्हें चार भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । इनकी रचना वैदिक काल में हुई, जब ऋषियों ने ब्रह्माण्ड के रहस्यों को समझने के लिए तपस्या और ध्यान के माध्यम से “श्रुति” (ईश्वरीय वाणी) को सुना और उसे मंत्रों के रूप में संकलित किया। इन वेदों के भीतर एक लाख मंत्र समाहित हैं। इनको समझने और उनके अर्थ को आत्मसात करने वाले ऋषियों को “मंत्र दृष्टा” कहा जाता है। मंत्रों को तीन मुख्य कांड में विभाजित किया गया हैं, जो मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों को समझाते हैं।
1- कुंभ और वेदों का तात्विक संबंध
कुंभ मेला चार स्थानों पर आयोजित किया जाता है – प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। कुंभ के आयोजन का मुख्य आधार वैदिक ज्ञान और ज्योतिषीय गणनाएं हैं। माना जाता है कि कुंभ का आयोजन उस समय किया जाता है जब ग्रह-नक्षत्र एक विशेष संयोग में होते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
कुंभ के दौरान वेदों का महत्व
कुंभ में वेदों के मंत्रों का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। इन मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है और व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वेदों में नदियों को पवित्र मानते हुए उनमें स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कुंभ के दौरान यह परंपरा जीवंत होती है।
कुंभ में ऋषि-मुनि और संत वेदांत का प्रचार करते हैं, जिससे आध्यात्मिक जागरूकता फैलती है। वेदों के मुख्य तीन कांड – ज्ञानकांड, कर्मकांड और उपासनाकांड – कुंभ मेले के आयोजन का भी सार हैं। वेदों के भीतर समाहित मंत्रों को तीन मुख्य कांड (खंड) में विभाजित किया गया है। ये कांड जीवन के अलग-अलग पक्षों और उद्देश्यों को समझाते हैं। कर्मकांड: यज्ञ, तप और पवित्र स्नान का महत्व बताता है। उपासनाकांड: ईश्वर की उपासना व भक्ति का मार्ग दिखाता है। ज्ञानकांड: आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित करता है।
a-कर्मकांड (80,000 मंत्र)। कर्मकांड जीवन के कर्म,यज्ञ और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए, कौन-सा कर्म श्रेष्ठ है और किस प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए। ये कर्म मुख्य रूप से यज्ञ, पूजा, स्वाध्याय (अध्ययन) और धर्म के पालन से जुड़े होते हैं। कर्मकांड का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखना और धर्म का पालन करना है।
b- उपासना कांड (16,000 मंत्र)। उपासना का अर्थ है परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से आत्मा को जोड़ना। इसमें भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा और निष्काम कर्म पर बल दिया गया है। यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण, विश्वास और भक्ति कैसे बढ़ाई जाए। उपासना कांड का मुख्य उद्देश्य है मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान।
c- ज्ञानकांड (4,000 मंत्र)। ज्ञानकांड मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति व स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। ये चार हजार मंत्र सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली हैं और ज्ञान का सार प्रदान करते हैं। इसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि और जीवन के सत्य को जानने की शिक्षा दी गई है। ज्ञानकांड का उद्देश्य आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान प्राप्त करना है।
ज्ञानकांड का महत्व
ज्ञानकांड वेदों का वह खंड है जो मानव जीवन में विवेक, समझ और निर्णय क्षमता को विकसित करता है। यह खंड हमें बताता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करता है। ज्ञान सबसे पवित्र और शक्तिशाली वस्तु है। यह मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है- “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।” अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह वाक्य दर्शाता है कि ज्ञान मानव जीवन को शुद्ध, जागरूक और सार्थक बनाता है।
ज्ञान व्यक्ति को विवेकशील और समझदार बनाता है। यह सही और गलत में अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा और दिशाहीन होता है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को भूलकर भटक जाता है। ज्ञान ही वह प्रकाश है, जो मानव को अंधकारमय जीवन से बाहर निकालकर उन्नति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तो उन्हें धन, संपत्ति या भौतिक सुख नहीं, बल्कि बुद्धि का उपहार देते हैं। यह बुद्धि “ज्ञान दीप” के रूप में प्रकट होती है, जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। बुद्धि और ज्ञान का संयोग हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सार्थक ढंग से जीने की शक्ति प्रदान करता है।
2- उपनिषद और ज्ञानकांड का उद्देश्य
उपनिषद वेदों के गूढ़ तत्वों का सार हैं, जो आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों को समझाते हैं। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य अध्यात्मिक ज्ञान को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना है। यह हमें आत्म-तत्व को जानने और ब्रह्म (परम सत्य) के साथ आत्मा के संबंध को समझने में मदद करता है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और माया (भौतिक संसार) में उलझना हमारे अज्ञानता का प्रतीक है। ज्ञानकांड मानव जीवन में ज्ञान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यह सिखाता है। जीवन के हर कार्य में ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए। सही और गलत का भेद समझकर उचित निर्णय कैसे लिया जाए। विवेकपूर्ण जीवन ही ज्ञान का सच्चा प्रयोग है।
ज्ञानकांड आत्मा के सत्य स्वरूप, मन की शक्ति और बुद्धि के रहस्यों को प्रकट करता है। यह सिखाता है कि मनुष्य के भीतर ही आत्मज्ञान का दीपक है, जिसे जाग्रत करने की आवश्यकता है। ज्ञान ही मानव जीवन का आधार और सबसे बड़ी पूंजी है। यह जीवन को दिशा और सार्थकता प्रदान करता है।
ज्ञान हमें केवल भौतिक उन्नति ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी दिखाता है। भगवान की कृपा से प्राप्त “ज्ञान दीप” ही जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। ज्ञान दीप के माध्यम से व्यक्ति अज्ञानता, भ्रम और कष्टों से मुक्त होकर सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ता है।
उपनिषद और ज्ञानकांड दोनों हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान ही जीवन का मार्गदर्शक और प्रकाश है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा और दिशाहीन होता है। उपनिषदों का चिंतन और ज्ञानकांड का अध्ययन हमें सत्य की अनुभूति कराता है और जीवन को पूर्ण, सार्थक और उज्ज्वल बनाता है। “ज्ञान ही परम शक्ति है, जो मानव को ईश्वर के समीप ले जाती है और उसके जीवन के हर अंधकार को दूर करती है।”
3- कुंभ: आत्मा, शक्ति और ज्ञान का संगम
कुंभ मेला चार स्थानों (प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक) पर आयोजित होता है। इसका आयोजन वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थितियों के आधार पर किया जाता है। यह एक खास स्थित है, जब गुरु ग्रह (बृहस्पति) सिंह राशि में प्रवेश करता है, तो यह एक विशेष संयोग बनाता है। गुरु का तात्पर्य ज्ञान से है, जबकि सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस संयोग का गूढ़ अर्थ है कि ज्ञान (गुरु का तेज) और शक्ति (सिंह का बल) के मेल से जीवन में ऊर्जा, संतुलन और दिशा का संचार होता है।
कुंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन की पूर्णता केवल शारीरिक बल या भौतिक सुखों से नहीं होती। इसके लिए ज्ञान का प्रकाश और आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्ञानकांड का यही संदेश है कि सच्ची संतुष्टि और उन्नति केवल विवेकपूर्ण ज्ञान से ही संभव है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, शक्ति संचय और ज्ञान प्राप्ति का पर्व है। यहां आने वाले साधु-संत और श्रद्धालु ज्ञान की खोज में आते हैं ताकि उनकी आत्मा को नई दिशा और ऊर्जा मिल सके।
कुंभ का आयोजन वेदों और उपनिषदों के मूल तत्वों पर आधारित है। कुंभ हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य – ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक उत्थान की ओर प्रेरित करता है। कुंभ मेला ज्ञानकांड के मूल सिद्धांतों को जीवंत करता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का संगम जीवन को सार्थक बनाता है। केवल बाहरी बल नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान और विवेकपूर्ण ज्ञान ही सच्चे सुख और संतोष का मार्ग है। इस प्रकार, कुंभ मेला आत्मा, शक्ति और ज्ञान का संगम है, जो हर व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, दिशा और प्रकाश का संचार करता है।
प्रयागराज की भूमि केवल एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। यह भूमि हिमालय की पवित्रता, गंगा के प्रवाह और ऋषि-मुनियों की तपस्या का प्रतिफल है। गंगा, जो हिमालय से निकलती है, अपने प्रवाह में पर्वतों, जंगलों, पत्थरों और औषधीय गुणों वाली मिट्टी को साथ लाती है। यह मिट्टी 12 वर्षों तक लगातार संग्रहित होकर प्रयागराज की भूमि को तपोभूमि में परिवर्तित करती है।
प्रयागराज का कुंभ मेला केवल संगम की पवित्रता का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हिमालय की तपोभूमि का प्रतीक है। साधु-संतों की साधना और ज्ञान-तप का जीवंत उदाहरण है। यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति को जीवंत करता है। प्रयागराज कुंभ ज्ञान-भक्ति-शक्ति का संगम है। यह मेला अद्वितीय है, क्योंकि इसमें साधु-संतों के प्रवचनों, ज्ञान साधना और वैदिक परंपराओं का प्रसार होता है।
यहां भक्ति का प्रवाह है। श्रद्धालु पवित्र स्नान और पूजा-अर्चना कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से मनुष्य को नई दिशा और शक्ति मिलती है। प्रयागराज कुंभ की पवित्रता और विशेषता इसे अन्य तीन कुंभ स्थलों (हरिद्वार, उज्जैन और नासिक) से अलग बनाती है। यहां तीनों नदियों का संगम (गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती) होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह संगम आत्मा, मन और बुद्धि के शुद्धिकरण का प्रतीक है।
कुंभ मेला में साधुओं की उपस्थिति
कुंभ मेला में विभिन्न प्रकार के साधु-संत और संन्यासी आते हैं, जो अपनी-अपनी विशिष्ट साधना पद्धति और कार्यक्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन साधुओं की उपस्थिति कुंभ मेला को एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र बनाती है, जहां भक्त और साधक आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकत्रित होते हैं।
कुंभ मेला में दसनाम साधुओं की उपस्थिति केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। ये साधक निम्नलिखित माध्यमों से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं और दूसरे को इसके लिए प्रेरित करते हैं। इन साधुओं की तपस्या, साधना और परमहंस की अवस्था कुंभ मेला की ऊर्जा और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती है। वेदों के ज्ञानकांड और उपनिषदों के सिद्धांतों के अनुरूप, कुंभ मेला आत्मा, शक्ति और ज्ञान का संगम है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक विकास और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है।
साधुओं के दस प्रकार
पुरी : नगरों में रहकर धर्म का प्रचार-प्रसार करना। इनका मुख्य कार्य शास्त्रों का अध्ययन और शिक्षण, गीता और वेदों का प्रवचन, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन। समाज में धर्म और नैतिक मूल्यों का प्रसार करना।
गिरि : पर्वतों पर रहकर तपस्या और साधना करना। इनका मुख्य कार्य सूर्य की उपासना, आत्म-निर्माण और ज्ञान-संवर्धन। आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शक्ति का विकास।
भारती : शिक्षा और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। इनका मुख्य कार्य शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा देना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण। समाज में ज्ञान और शिक्षा के महत्व को स्थापित करना।
बन : जंगलों में रहकर तपस्या करना। इनका मुख्य कार्य छोटे बगीचे बनाना, पशुओं की देखभाल, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। प्रकृति के साथ एकाकार होकर आत्मा की शुद्धि करना।
सरस्वती : ज्ञान के वाहक, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन। इनका मुख्य कार्य शास्त्रों का अध्ययन और दूसरों को शिक्षित करना। ज्ञान के प्रसार और आत्मज्ञान की प्राप्ति।
आरण्यक : जंगलों में मचान बनाकर या बर्फीले क्षेत्रों में साधना करना। इनका मुख्य कार्य औषधियों और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके तपस्या करना। प्रकृति के तत्वों के साथ साधना करके आत्मा की शुद्धि करना।
पर्वत : बर्फ के बीच साधना करना। इनका मुख्य कार्य सूर्य की आराधना में लीन रहना। इनका मकसद उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना।
तीर्थ : तीर्थ स्थलों का भ्रमण और धार्मिक स्थलों का संरक्षण। इनका मुख्य कार्य तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक स्थलों की रक्षा और देखभाल। धार्मिक स्थलों के महत्व को बढ़ावा देना और उनकी शुद्धि करना।
धाम : धार्मिक धामों में भ्रमण करते हुए साधना करना। इनका मुख्य कार्य विभिन्न धामों की यात्रा और साधना करना। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों का अनुभव करना।
पीठ : पीठ स्थलों (जैसे चार धाम) में आध्यात्मिक यात्रा और साधना करना। इनका मुख्य कार्य चार धामों की यात्रा करना और साधना करना। उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव और मोक्ष की प्राप्ति।
ब्रहनिष्ठ संतोष पुरी (स्रोतीय, ब्रहनिष्ठ, परिव्राजक, परमहंस, दशनाम संन्यासी, पुरीनाम, मुल्तानी मढ़ी, बराह देवता, कामाख्या पीठ, रामेश्वरम धाम, महानिर्वाणी अखाड़ा) के विचार